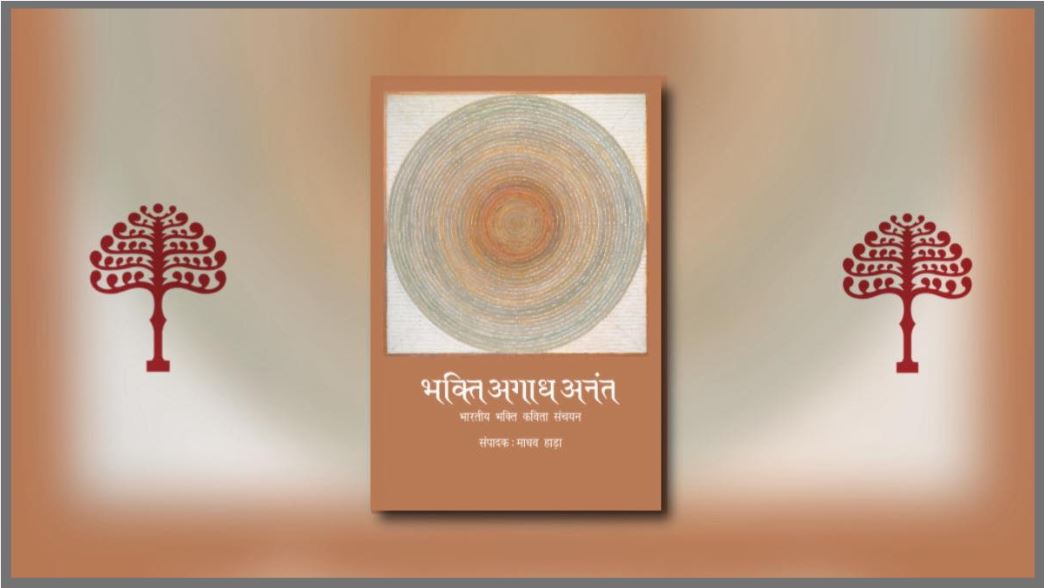भक्ति भारतीय चेतना का वह आत्मस्वर है, जिसने ज्ञान, लोक और सौंदर्य के मध्य सेतु की तरह कार्य किया. हमारी ज्ञान परंपरा में भक्ति केवल एक भाव भर नहीं है, बल्कि चेतना रूपांतरण समाज सुधार और आत्मान्वेषण का माध्यम भी है.
आज जब चारों ओर से विस्थापन, अकेलापन और अस्तित्वगत संकट हमें घेरे हैं, ऐसे समय में, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की जरूरत है. साहित्य के क्षेत्र में वह सामान्य संग्रहों के बजाय ऐसे सांस्कृतिक-अध्यात्मिक दस्तावेजों से घटेगा, जो आधुनिक मनुष्य की आत्मरिक्तता की पहचान करें.
अपनी संरचना और गठन में समानता और प्रतिरोध का उत्तेजक नहीं, प्रेरक स्वर बने. जो लोक और शास्त्र दोनों का संगम हो तथा जनभाषाओं की गरिमा भी बचाए रखे. जो केवल किसी साहित्यिक परंपरा का पुनर्संयोजन भर न हो, बल्कि उसमें धर्म की मानवीय गरिमा भी व्याख्यायित हो.
माधव हाड़ा द्वारा संपादित ‘भक्ति अगाध अनंत’ एक ऐसा ही संचयन है, जिसकी आवश्यकता लंबे समय से केवल अकादमिक संस्थानों या सुधि साहित्यिकों को नहीं थी वरन् जिसकी सर्वाधिक जरूरत रसहीन होते जा रहे सहृदय समाज को थी.
संचयन में पहली बार, छठी शताब्दी से लेकर आधुनिक काल के सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ तक, लगभग सभी भारतीय भाषाओं के 50 प्रतिनिधि कवियों को 736 पृष्ठों में एक स्थान पर संकलित किया गया है. 55 पृष्ठों की ‘भारतीय भक्ति चेतना पहचान, व्याप्ति और वर्गीकरण का पुनरवलोकन’ शीर्षक से आई भूमिका भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है.
यह संचयन देशज भक्ति परंपरा का अनुभव द्वार है, जिसमें बहुत ही स्पष्ट ढंग से भारतीय एवं पश्चिमी भक्ति अवधारणा और उससे संबंधित संशयों के निराकरण का उचित प्रयास है. दरअसल, अब तक के भक्ति अध्ययनों ने भक्ति की मूल अवधारणा को विदेशी दृष्टि से देखा, जांचा और परखा. हाडा का प्रयास पहली बार विउपनिवेशित दृष्टि से अपनी परंपरा के साथ सहज संवाद है.
भारतीय भक्ति चेतना की व्याख्या
संपादक ने पश्चिमी ज्ञान मीमांसा और पूर्वी ज्ञान मीमांसा के भेद को आत्मगत कर उनके बीच की अस्पष्ट खाई को स्पष्ट रूप से लक्षित करते हुए भारतीय भक्ति चेतना को व्याख्यायित करने में सफलता अर्जित की है. पश्चिम की भक्ति का स्वर ईश्वर की कृपा (grace), व्यक्तिगत नैतिकता और प्रार्थना के रूप में उभरता है, जबकि भारत में यह लोक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, और सौंदर्यपूर्ण रूपों में अधिक गहराई से विकसित हुआ.
पाश्चात्य भक्ति परंपरा के आधार सेवा पाप-कृपा सिद्धांत, ईश्वर प्रेम रहे हैं, वहीं भारतीय भक्ति चेतना का आधार आत्मा-ब्रह्म एकता, प्रेम रहा है. पश्चिमी भक्ति परंपरा की भाषा नैतिक, व्यक्तिगत, प्रार्थनात्मक है वहीं हमारी भक्ति चेतना की भाषा सांस्कृतिक, सांगीतिक, लौकिक है.
उनकी भक्ति परंपरा का माध्यम चर्च, बाइबिल, प्रार्थना, गाना आदि है, वहीं भारतीय भक्ति परंपरा का माध्यम कीर्तन, जप, योग, साहित्य आदि है. उनकी दृष्टि विश्वास से उद्धार की रही है जबकि हमारी प्रेम ही मोक्ष है की रही है.
किसी रचना या आलेख का शीर्षक केवल नाकरण की परंपरा का निर्वाह भर नहीं होता है. वरन यह उस सर्जक की अनुभव की यात्रा का प्रवेश द्वार भी है, जो बताता है कि आगामी रचनात्मक यात्रा किस लोक, विचार या दृष्टि चैतन्य की ओर जाएगी.
इस अर्थ में शीर्षक भक्ति चेतना पहचान, व्याप्ति, वर्गीकरण का पुनरवलोकन समूचे संचयन के विचार को एकसूत्र में पूरी तरह स्पष्ट कर देता है.
संत दादू की काव्यपंक्ति ‘भक्ति अगाध अनंत’ इस संचयन के पाठक की रचनात्मक के साथ व्याख्यात्मक भागीदारी को भी बढ़ाने वाला है. यह अर्थ को तो जोड़ता ही है, साथ ही आस्वाद की गहराई को भी बढ़ाता है जिसका माध्यम एक ऐसा आत्म उजास है जो पूरे पाठ प्रांगण के कोने-कोने को आलोकित किए है.
पूरे संचयन से गुजरने पर भक्ति यहां उपासना की नहीं अस्तित्व की पहचान के रूप में उभरकर आती है. अगाध पद उसी भक्ति को सागरीय गरिमा प्रदान करता है. ऐसी गहराई जो अगाध है, अथाह है, और अनंत यानी सीमाविहीन. यानी तीनों पद मिलकर एक विशिष्ट राह संधान करते हैं जो एकत्व, गहराई, व्यक्तिगत, विस्तार, सार्वभौमिकता का समाहार स्वयं किए है.
इन अर्थों में ‘भक्ति अगाध अनंत’ एक शीर्षक भर नहीं रह जाता, वरन् मानवीय चेतना की एक विशिष्ट उपमा के रूप में उभरकर आता है जो हमारे भीतर जितनी गहरे उतरती है समाज में उतनी ही दूर तक फैल भी जाती है.
दर्शन, तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा
संचयन के प्रारंभ में आया 55 पृष्ठीय आकलन इसका प्राणतत्त्व है. यहां गौर करने वाली बात यह है कि हाड़ा ने पहचान, व्याप्ति और वर्गीकरण तीन पदों का चयन किया. प्रश्न उठता है कि इन तीन पदों का ही चयन क्यों?
इसके उत्तर की तलाश में और इन तीनों पदों की पारस्परिकता को समझने के लिए हमें दर्शन, तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा के स्तर पर जाकर देखना होगा. थोड़ा ठहरकर गौर करेंगे, तो पाएंगे कि तीनों ही मूलतः एक दूसरे से अलग दिखते हुए भी परस्पर गहरे निबद्ध हैं.
ऊपर भारतीय भक्ति चेतना और नीचे पहचान,व्याप्ति और वर्गीकरण का पुनरावलोकन उपशीर्षक दर्शाता है कि संपादक के पास एक अखंड दृष्टिबोध और तार्किक प्रवाह की लय है. अपने कुशल संपादन से उसने सबको एकसूत्र में पिरो दिया है.
पहला पद पहचान यानी स्वरूप निश्चय (तर्कशास्त्र) अर्थात् यह वही है कुछ और नहीं. दूसरा पद व्याप्ति यानी सह-अस्तित्व, नियत संबंध- जैसे धुआं-अग्नि. एक अविभाज्य संबंध. यही व्याप्ति है. गौर कीजिए पहचान का संबंध क्या है से है और व्याप्ति का किससे से है. यानी व्याप्ति पहचान से आरंभ हुई यात्रा का दूसरा पड़ाव है.
और तीसरे पड़ाव का उदय इन दो चरणों से गुजरने पर ही होगा. जब क्या, किससे का प्रश्न शांत होगा, तभी क्रमबद्धीकरण या व्यवस्थापन की प्रक्रिया को गति मिलेगी. तर्कशास्त्र की दृष्टि से इस यात्रा को देखें तो निश्चय अनुमान और सामान्यीकरण और विज्ञान के आलोक से देखें, तो तत्त्व की खोज, अभिक्रियाएं और सारणी.
हालांकि, संपादक इन सभी का समाहार अपनी सांस्कृतिक दृष्टि में करते हुए इन पदों को अपनी अनुभव यात्रा का भक्ति साहित्य के विशेष संदर्भ में हिस्सा बनाते हुए आगे बढ़ता है. पहचान यानी स्व-बोध अर्थात् मैं कौन हूं. व्याप्ति यानी परस्परता अर्थात् मैं – वह का संबंध. वर्गीकरण यानी व्यवस्थापन आर्थात् समूहों, वर्ग समानता आदि.
विशद अध्ययन एवं प्रामाणिक संदर्भ
इस दृष्टि से देखने पर हम पाएंगे कि पहचान अलगाती है, व्यप्ति जोड़ती है और वर्गीकरण व्यवस्थित करता है. तीनों मिलकर ज्ञान की प्रक्रिया को संपूर्ण बनाते हैं. यानी भक्ति चेतना के अखंड चैतन्य को हमारे सम्मुख रखते हैं. इसलिए संपादक ने इनका चयन किया है.
संपादक अपने विशद अध्ययन एवं प्रामाणिक संदर्भों के साथ भक्ति चेतना और साहित्य की पहचान पर लंबे समय से आए कुहासे को छांटते हैं. यह कुहासा सदियों पुरानी परंपरा के रूप में समादरित रहा है.
अतः पश्चिमी ज्ञान मीमांसा के दार्शनिक धरातल पर जाकर वे भारतीय मनीषा की सहज वाणी में उसके साथ संवाद कर उसे साफ करने की पहल करते हैं.
वे जार्ज ग्रियर्सन द्वारा प्रस्तुत इस विचार को खारिज करते हैं, जिसमें क्रांति के पर्याय रूप में आंदोलन का महत्त्व दिया गया. उनका अध्ययन बताता है कि भक्ति को सुधार, पुनरुत्थान, जागरण, पुनर्जागरण नहीं बल्कि वह हमारी परंपरा में प्रेम, समर्पण, निष्ठा, शरणागति स्तुति आदि से देखा जाना गया है.
इसी क्रम में वे भक्ति चेतना के उपलब्ध, वर्गीकरणों और विभाजनों से अपनी विनम्र किंतु तार्किक असहमति प्रकट करते हैं. क्योंकि उनके स्वीकार से भारतीय भक्ति चेतना की निरंतरता, वैविध्य, व्यापकता की सम्यक् पहचान बाधित होती है.
सगुण-निर्गुण की परंपरा
वे बार-बार सप्रमाण यह बताते चलते हैं कि उपलब्ध भक्ति-साहित्य, विगत शताब्दियों की परंपरा पश्चिमी ज्ञान मीमांसा की प्रेरणा से उपजी है. फिर उसके निर्माता चाहे विदेशी विद्वान हो या देसी सबकी दृष्टि पश्चिम की सृष्टि को मजबूत बनाने की राह पर ही आगे चली है.
सगुण-निर्गुण की परंपरा आवाजाही के संबंध में लगी पाबंदियों को वे रवींद्रनाथ ठाकुर के उदाहरण से समझाते है जिसमें वे लिखते हैं कि भारतवर्ष की ब्रह्मविद्या में हम दो धाराएं देखते हैं- निर्गुण ब्रह्मम और सगुण ब्रह्म, भेद और भेदाभेद. यह ब्रह्मविद्या कभी संपूर्ण रूप से एक की ओर झुकती है, कभी वह द्वैत को मानकर इसी द्वैत के बीच एक को देखती है.
वे स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि वर्तमान में उपलब्ध भक्ति चेतना का काल विभाजन भी युक्ति संगत नहीं है. क्योंकि यह भी बिना भारतीय चेतना की सांस्कृतिक परिस्थिति को समझे संरचित किया गया है.
वे 1318 से 1643 ई. तक बांटी गई अवधि को भक्ति चेतना के अजस्र प्रवाह को सीमित करने का उपक्रम करार देते हैं. वे बीसियों संतों के साहित्य प्रमाणों से बताते हैं कि भक्ति चेतना एक नैरन्तर्य में प्रवाहमान चेतना है. जिसका विस्तार आधुनिक काल तक जाता है.
कवि कुलगुरु रवींद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी को संभवतः पहली बार हिंदी साहित्य इतिहास में एक भक्त कवि के रूप में किसी संचयन में शामिल किया गया है.
भक्ति साहित्य से संबंधित समस्त मूल पूर्वाग्रहों के साथ उनकी निर्मिति को अमर्त्य सेन के हवाले से बताते हुए वे कहते हैं कि सेन ने उन्नीसवीं सदी के समस्त अध्ययनों एवं अनुसंधानों के विश्लेषण की विधियों को विदेश प्रेमी, दंडाधिकारी और संग्रहाध्यक्षीय तीन वर्गों में बांटा है.
अमर्त्य सेन के अध्ययन से ही वे बताते हैं कि ये विश्लेषण पूरी तरह निष्पक्ष नहीं रह पाए, इनमें एक रुझान से दूसरे दो रुझान भी किसी न किसी तरह अवश्य ही प्रभावित हुए हैं. अतः वे औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा द्वारा प्रस्तुत समस्त घटनाओं को पूर्वाग्रह से युक्त एवं आधारहीन करार देते हैं.
देशज भक्ति विमर्श की परंपरा
हिंदी में आचार्य शुक्ल की मान्यताएं भी कमोबेश इसी औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा का ही विस्तार है. इसलिए अधिकांश अध्येताओं ने देशज स्रोतों की प्रामाणिकता को संदेह से देखा.
हमारी अपनी देशज भक्ति विर्मश की परंपरा में इस चेतना के सतत् प्रवाह में 52 स्तम्भों (थांबे) की भूमिका को सर्वोपरि एवं महत्त्वपूर्ण देती है जबकि यहां ध्यान दिए जाने योग्य तथ्य यह भी है कि वे ताराचंद, हुमायूं, कबीर, आबिद हुसैन जैसे विद्वानों के अध्ययन से भी अपनी असहमति दर्ज करवाते है.
आगे यह भी बताते हैं कि इन दिग्गजों की मान्यताओं का कालांतर में दिनकर व हजारीप्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने इसका प्रतिवाद किया. हम कह सकते हैं कि उसके बाद प्रतिवाद का यह स्वर मात्रा में तो कम हुआ ही गुणवत्ता में कमजोर होता गया. अब इस संचयन ने उस मंद स्वर को एक आत्मदीप्ति और तेज प्रदान किया है.
हाड़ा अपने अध्ययन में प्रामाणिक स्रोतों, अस्पर्शी ग्रंथों का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय भक्ति चेतना में अंतःक्रियाओं और रूपांतरण की प्रक्रिया सदैव ही चलती रही है. हां, यह गति कभी मंद कभी तीव्र रही, पर इसकी निरंतरता को लेकर कोई संदेह है ही नहीं.
इस संदर्भ में वे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से पहले महानुभाव संप्रदाय के हवाले से प्रमाणित एवं स्पष्ट करते चलते हैं कि यह संप्रदाय विभिन्न धार्मिक परंपराओं का जटिल मिश्रण है.
भारतीय भक्ति चेतना की बहुवचनीयता
भारतीय भक्ति चेतना की सांस्कृतिक निर्मिति कुछ इस तरह से है कि उसे किसी सीमित कोण, विचार या संप्रदाय आदि में अटाया-घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वे अपने मूल में कई परंपराओं के संयोग एवं मिश्रण से बनीं हैं. बहुवचनीयता भारतीय भक्ति चेतना के संधान का एक ओर विशिष्ट गुण है. इसलिए उसमें मातृभाषा जैसी किसी गुंजाइश के बजाय देशभाषाओं की स्वीकृति और मान्यताओं को महत्त्व दिया गया है.
हाड़ा इस बहुवचनीयता के मूल में प्रतिरोध, समाहार, पृथक्करण, विस्तार को कारण रूप से में देखते हैं और भारतीय भक्ति चेतना को स्वतंत्रता, समता और न्याय की त्रयी के रूप में वे देखने-दिखाने की पुरजोर पहल करते हैं. इसी क्रम में वे देशज विमर्श की अपनी व्याख्या में भक्तिमाल पर भी परची ,बीतक, वार्ता आदि को जीवंत परंपरा के रूप में देखते हैं और उन्हें अपने तर्कों, प्रमाणों में पर्याप्त महत्त्व देना इतिहास के रिक्त स्थानों को भरते चलना हैं.
छठी शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक सतत् प्रवाहमान् रही निरंतरता को वे भक्ति चेतना तक ही सीमित करके नहीं देखते हैं बल्कि भारतीय चेतना के सार्वकालिक प्रमुख गुण के रूप में भी देखते हैं. इसी को रवींद्रनाथ ने भारतीय आत्मा की संज्ञा से अभिहित किया है.
संचयन की विशिष्टता इसमें भी है कि पहली बार लगभग सभी भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि रचनाकार और उनके साहित्य की प्रतिनिधि रचनाओं के चयन से उनका यह संचयन केवल कलेक्शन नहीं रह जाता वरन् सलेक्शन के रूप में हमारे सामने है.
यह अध्ययन यह भी स्थापित करता है कि हमें अपनी परंपरा के पुनरावलोकन की प्रक्रिया में बड़ी सजगता एवं सावधानी के साथ पर्याप्त धैर्य की जरूरत है. भारत एवं भारतीयता का स्वर एवं अन्वेषण इस संचयन का बीज स्वर है.
यह संचयन हिंदी भाषा की ज्ञान मीमांसा के स्वाभिमान को बदलने की दिशा में उठा एक मजबूत कदम है. कह सकते हैं कि हाड़ा ने विषय-सीमा, दृष्टि निर्धारण, वर्गीकरण, भाषा के साथ अपने चयन में रचनात्मकता के साथ-साथ अनुभव की गहराई और उनके असर पर भी पर्याप्त ध्यान दिया है.
(ब्रजरतन जोशी युवा आलोचक और कवि हैं, जो राजस्थान साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका ‘मधुमती’ के संपादक रहे हैं.)